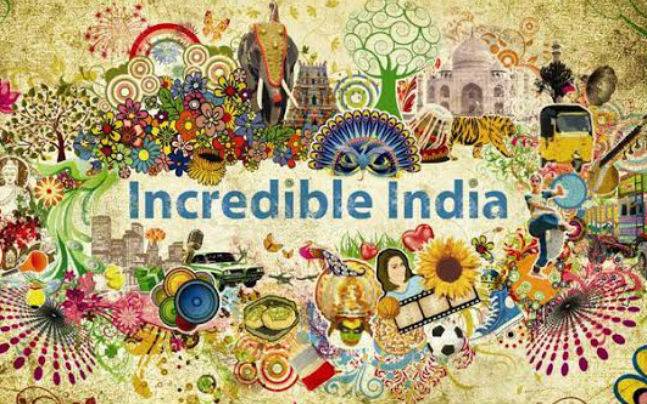
विविधता शब्द सुनते ही बरबस मेरा ध्यान तीन बातों की ओर खिंच जाता है – साम्राज्यवाद, राष्ट्रीय एकता से जुड़े संदेश और उदार बाज़ार व्यवस्था। ऐसे में मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैं संसार की मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अगर हम अनेक संभावनाओं वाली समावेशी राजनीति के संदर्भ में विविधता शब्द की बात करें, तो मेरे विचार से हमें यह जान लेना चाहिए कि, इस ओर इस शब्द को किस तरह से और किस प्रयोजन से प्रयोग में लाया जाता रहा है।
यूरोपीय यात्रियों के यात्रा वृतांत पढ़ने में मेरी हमेशा से रुचि रही है। विविधता के प्रति उनका आकर्षण मुझे हमेशा से ही सम्मोहित करता रहा है। यहाँ यह कहने का मेरा यह मतलब बिलकुल नहीं है कि यूरोपीय यात्रियों से पहले कभी कोई विविधता से आकर्षित ही नहीं हुआ था – ऐसा बिलकुल नहीं है। मेरा कहने का अर्थ केवल इतना है कि यूरोपियन लोगों ने, विशेषकर 19वीं और 20वीं शताब्दी के यात्रियों ने जिस तरह से विविधता को समझा, उससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हूँ। 19वीं और 20वीं शताब्दी आते-आते यूरोप की महिलाएँ भी अपने उपनिवेशों की यात्रा करने लगी थीं, और आमतौर पर उनकी ये यात्रा अपने लिए सुयोग्य यूरोपीय वर की तलाश में की जाती थीं। जैसा कि एन लौरा स्टोलर (Ann Laura Stoler) के बेहतरीन लेखों से पता चलता है, यूरोप की महिलाओं के इन औपनिवेशिक देशों में प्रवास से यह सुनिश्चित हो जाता था कि इन यूरोपीय पुरुष अधिकारियों से पैदा होने वाली संतान मिश्रित प्रजाति की न होकर विशुद्ध यूरोपीय ही होती थी। अपनी पुस्तक रेस एंड द एजुकेशन ऑफ़ डिजायर (Race and the Education of Desire) में उन्होने नस्लीय शुद्धता को बरकरार रखने पर यूरोप की साम्राज्यवादी सत्ता की चिंताओं की ओर ध्यान खींचा है। मानव की विभिन्न नस्लों के बीच के अंतर और विशेष नस्लों के दूसरों से बेहतर होने के अध्यन्न के एक विज्ञान रूपी विषय की तरह उभरने के साथ ही यह कहा जाने लगा था कि श्वेत नस्ल के लोग न केवल सांस्कृतिक रूप से अधिक उन्नत होते हैं बल्कि वे शारीरिक रूप से भी दूसरी नस्लों की तुलना में बेहतर हैं। इस विचारधारा के बलवती होने का परिणाम यह हुआ कि श्वेत पुरुषों द्वारा, चाहे वे साम्राज्य के किसी भी उपनिवेश में तैनात हों, केवल श्वेत संतान को पैदा करना ही महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। बड़ी संख्या में यूरोपीय महिलाओं द्वारा साम्राज्य के अधीन उपनिवेशों में तैनात पुरुषों के साथ विवाह करने और पैदा होने वाली संतान की परवरिश करने के लिए इन उपनिवेशी देशों में प्रवास करना शुरू कर देने के बाद, श्वेत पुरुषों, श्वेत महिलाओं, अश्वेत पुरुषों और अश्वेत महिलाओं के बीच यौन सम्बन्धों की सामाजिक मान्यता पर चर्चा होनी शुरू हो गयी। इस नज़रिए में उपनिवेशों में तैनात श्वेत पुरुषों के संपर्क में आने वाली अश्वेत महिलाओं को इन पुरुषों का शोषण करने वाली और पैदा होने वाली मिश्रित नस्ल की संतान की माँ बन जाने जैसे जोखिम के रूप में देखा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर, अश्वेत पुरुषों को श्वेत महिलाओं का शोषण और उनके साथ हिंसा करने के संभावित खतरे के रूप में समझा जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशों में श्वेत और अश्वेत लोगों के सार्वजनिक और निजी स्थानों पर, एक दूसरे के संपर्क में आने के बारे में कड़े कानून बनाए जाने लगे और उनके परस्पर मेल-जोल पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी।
धारा 377 पर लगातार हुई चर्चा से हम जानते ही हैं कि, 19वीं शताब्दी ही वो समय था जब संतान पाने के उद्देश्य से किए जाने वाले सेक्स के अलावा दूसरी सभी तरह की यौन प्रवृत्तियों को गलत, अनैतिक और आपराधिक करार दिया गया था। ऐसे में जब नस्लीय श्रेष्ठता पर चल रहे विचारों के तहत जहाँ जहाँअलग-अलग नस्लों के बीच संबंध बनाने की इच्छा पर भी लोगों में राय कायम होने लगी थी, वहीं यौन इच्छाओं को आपराधिक और असामान्य माने जाने के नज़रिए के तहत हर नस्ल के मनुष्यों में जेंडर के आधार पर ‘सामान्य’ समझे जाने वाले यौन रुझानों को भी परिभाषित करने की कवायद चल पड़ी थी। नस्ल और इच्छाओं की इन दोनों विचारधाराओं के एक साथ प्रभावी होने का नतीजा यह निकला कि गैर-विषमलैंगिक और अंतर-नस्लीय संबंध बनाने की इच्छाओं को ही अप्राकृतिक और अनैतिक मान लिया गया। चूंकि उस समय साम्राज्यवादी ताकतों का पूरा ध्यान अपने मुख्य नागरिकों, अर्थात श्वेत पुरुषों के “स्वास्थ्य” को सुरक्षित रखने पर था, इसलिए अश्वेत पुरुष शरीर को न केवल श्वेत महिलाओं, बल्कि श्वेत पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा मान लिया गया। श्वेत महिलाओं से जहाँजहाँ यह उम्मीद की जाती थी कि वे दाम्पत्य जीवन के उच्चतम आदर्श साबित हों, वहीं अश्वेत महिलाओं की ओर भी दो कारणों से विशेष ध्यान दिया जाने लगा। ऐसा समझा जाता था कि खुले में सेक्स के लिए ग्राहक ढूँढने से लेकर उत्तेजक नाच-गाने के खिलाफ़ कानून बना कर न केवल इन अश्वेत महिलाओं को खुद अपनी यौनिकता का शिकार होने से बचाया जाना ज़रूरी है बल्कि इन क़ानूनों के द्वारा उन्हें अश्वेत पुरुषों के शोषण से भी सुरक्षित रखे जाने की ज़रूरत है। उपनिवेश बनाए गए देशों में उस समय पितृसत्ता व्यवस्था के अधीन बाल-विवाह, घरेलू हिंसा और सती जैसी सांस्कृतिक रूप से मान्य प्रथाओं का चलन था और इनके माध्यम से महिलाओं का शोषण होता था। ऐसा लिखने से यहाँ मेरा यह तात्पर्य बिलकुल भी नहीं है कि मैं इन क़ानूनों के बनाए जाने से भारत में महिला स्शक्तिकरण में हुई बढ़ोत्तरी को, या अश्वेत पुरुषों और महिलाओं, दोनों के उदारवादी नारीवादी राजनीति में शामिल हो जाने को किसी भी तरह से कम करके आंकना चाहती हूँ। मैं यहाँ केवल इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि कुछ विशेष “संस्कृतियों” के बारे में ही ऐसा सोचा जा रहा था कि उनमें हिंसक और मनमाने अनैतिक व्यवहार करने की प्रवृति अधिक है। इस तरह, जहाँजहाँ एक ओर यौनिकता को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए क़ानूनों से नस्ल विशेष के बारे में कुछ खास तरह की मान्यताओं को जेंडरीकृत कर दिया वहीं इन क़ानूनों के बारे में भी इसी तरह की सोच विकसित होने लगी।
एक ओर जहाँजहाँ, साम्राज्यवादी शासन ने एक विशेष तरह की नस्ल श्रेष्ठता और पारिवारिक परंपरा को बनाए रखने के लिए विविध यौन रुझानों को कुचला, वहीं मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि किस तरह इसी साम्राज्यवादी सत्ता ने इस शब्द “विविधता” को अंगीकार किया। श्वेत पुरुषों द्वारा यौन इच्छाएँ रखने और साम्राज्य के लाभ के लिए “उत्तम संतान पैदा किए जाने” को ध्यान में रख कर कानून बनाते समय, साम्राज्यवादी शासकों का उद्देश्य यह भी था कि अपने इन उपनिवेशों को भौतिक और सांस्कृतिक तरीके से अलग-अलग श्रेणियों और वर्गों में बांटा जाए। ऐसे में जहाँजहाँ कुछ विशेष तरह की विविधता को जहाँजहाँ दबाया जा रहा था, वहीं सत्ता, जेंडर आधारित व्यवस्था तैयार करने के लिए, तितलियों से लेकर मनुष्यों तक, हर दूसरी हर तरह की विविधता की श्रेणियाँ तैयार करने में लगी थी और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प थी कि भौतिक रूप से केवल दो ही तरह के जेंडर की श्रेणियाँ संभव थीं। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र, जहाँजहाँ मैं काम करती हूँ, के चित्रों में दिखाया जाता है कि किस तरह अलग-अलग जाति के लोगों के कपड़े पहनने, गहने पहनने, बदन पर गोदना और छेद कराने के तरीके एक दूसरे से अलग थे। प्रत्येक प्रजाति में भी, पुरुषों और महिलाओं, लड़के और लड़कियों, अविवाहित और विवाहित महिलाओं के बीच इन वस्तुओं के प्रयोग का तरीका अलग था। इस सबके द्वारा नस्ल के आधार पर जेंडर और यौनिकता में भी भेद होना बताया गया था – और यह सब करने का उद्देश्य था कि ऐसा कर साम्राज्य के उपनिवेशों में जातिय विविधता को तो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए परंतु जेंडर की अनेक विविधताओं को किसी तरह से छिपा दिया जाए। स्त्री और पुरुष के अलावा समाज में प्रचलित किसी अन्य तरह की जेंडर विविधता का अध्यन्न केवल नाममात्र समझने या बिलकुल न समझने के उद्देश्य से ही किया गया।
भारत में – दरअसल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में – यह पूरा वर्गीकरण साम्राज्यवाद के समय से भी पहले से व्याप्त ज्ञान और जानकारी से प्रभावित हुआ। यहाँ पहुँचने वाले ब्रिटिश यात्रियों और मानवविज्ञानियों ने केवल अपनी जानकारी के आधार पर अपने निष्कर्ष नहीं निकाले; बल्कि उन्होंने स्थानीय शोधकर्ताओं के शोध नतीजों के आधार पर भी अपने निष्कर्ष निकाले। यह स्थानीय शोधकर्ता आमतौर पर शासक वर्ग, ऊंची प्रभावी जाति या जनजातिय कबीलों के पुरुष ही होते थे। शोध किए जा रहे लोगों के बीच इन इनकी स्थिति और साम्राज्य की सत्ता के साथ इनके सम्बन्धों के आधार पर उस समय के साम्राज्यवादियों ने उपमहाद्वीप में नस्ल, जेंडर मान्यताओं और यौनिकता के बारे में अपने विचार कायम किए। इस तरह से साम्राज्यवाद से पहले प्रचलित मान्यताओं के आधार पर ही समाज का साम्राज्यवादी वर्गीकरण हुआ – और पहले से मान्य विचार, नस्ल और जेंडर के बारे में इस नयी साम्राज्यवादी विचारधारा का हिस्सा बनते चले गए। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राय: पहले से मौजूद मानकों और प्रथाओं के आधार पर ही साम्राज्यवादी सोच का विकास हुआ जिसमें जेंडर, नस्ल और जाति से जुड़े वर्ग-विभाजन शामिल होते चले गए।
स्वाधीनता मिलने पर जहाँ भारत को यह सभी जटिल ज्ञान और जानकारी विरासत में मिलीं, वहीं एक नए देश के निर्माण का दायित्व भी इसे विरासत में ही प्राप्त हुआ। इस नए स्वाधीन हुए देश को पहले ही इसकी विविधता की जानकारी दे दी गयी थी, लेकिन अब इसके सामने संगठित बने रहना सीखने की भी चुनौती थी। उस समय उभरते हुए मीडिया की अनेक विधाएँ जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें, रेडियो प्रसारण, टेलिविजन, सिनेमा, इश्तेहार, यातायात के सार्वजनिक वाहन, यहाँ तक कि स्कूलों के पाठ्यक्रम भी “विविधता में एकता” के उस संदेश को पहुंचाने के माध्यम बन गए जिसे देखते और सुनते हुए हम सब बड़े हुए हैं। इस संदेश से हम सब को देश में मौजूद सांस्कृतिक विविधता का तो पता चलता है लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं बताया जाता कि किस तरह से यह विविधता देश में जाति सम्बन्धों और जेंडर सम्बन्धों को प्रभावित करती है। इस संदेश के ज़रिए हमें यह नहीं बताया जाता कि अधीन रह चुके उपनिवेश देशों में प्रचलित जेंडर भूमिकाएँ भी विभिन्न औपनिवेशिक संस्कृतियों की विविधता के बारे में उस साम्राज्यवादी सोच का ही परिणाम हैं जो हमें बताती है कि आदर्श भारतीय पुरुष या महिला को कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या पहनना, ओढ़ना चाहिए, उनका खानपान कैसा हो और वे किस तरह की इच्छाएँ अपने मन में पालें। यही साम्राज्यवादी सोच हमें भारत के लोगों में परस्पर अंतर की भी जानकारी देती है कि कैसे भारत के मुसलमान, क्रिश्चियन या जनजाति के लोगों का पहनावा, खानपान और इच्छाएँ यहाँ के आम भारतीय पुरुष और महिला से अलग हैं। ये मान्यताएँ न केवल जेंडर भूमिकाओं को फिर से दोहरा कर पक्का करती हैं बल्कि यह भी कि भारत में ऊंची जाति के हिन्दू की केवल सामान्य भारतीय हैं और बाकी सभी उनसे भिन्न हैं और यही भारत की विविधता है।
साम्राज्यवादी शासन काल में जिन मान्यताओं और आपराधिक क़ानूनों ने नस्ल की विविधता, उसकी श्रेष्ठता की सोच को पक्का किया, उन्हीं मान्यताओं ने स्वाधीन भारत में भी सामाजिक और कानून प्रक्रिया को प्रभावित करना जारी रखा। यौन हिंसा पर प्रचलित विचारधारा के तहत आज भी अलग-अलग जाति के लोगों को अलग नज़रिए से देखा जाता है। पूरे देश में, लोगों को तब तनिक भी आश्चर्य नहीं होता जब उन्हें बताया जाता है कि यौन हिंसा करने वाला कोई पुरुष किसी नीची जाति या श्रेणी का है। इसी तरह कानून को लागू करने वाले अधिकारियों के लिए किसी शहर के खास हिस्से में अनैतिक या गलत यौन व्यवहारों को रोकने के लिए जाति और वर्ग या श्रेणी को आधार बना कर कार्यवाही करना कोई नयी बात नहीं है। इसलिए यह देखा गया है कि यौनिकता को कानून के द्वारा नियंत्रित करते हुए प्राय: जातिगत समीकरण फिर से देखने को मिलते हैं। किसी जाति विशेष पर निगाह रखने या उसे नियंत्रण में रखने की कोशिश में अक्सर यौनिकता पर नियंत्रण की कोशिश भी शामिल रहती है – उदाहरण के लिए अंतर्जातीय सम्बन्धों और विवाह को रोकने की कोशिश करने वाले लोग आमतौर पर अलग-अलग जाति के लोगों के एक साथ होने को रोकने की ही कोशिश में लगे होते हैं और उनका ध्येय वास्तव में अपनी जाति की श्रेष्ठता और प्रवित्रता को बचाना होता है। यहाँ मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि अंतर्जातीय सम्बन्धों के प्रति बैर या द्वेष के लिए साम्राज्यवाद ही उत्तरदाई है, बल्कि मेरा अभिप्राय केवल यह रेखांकित कर देना है कि साम्राज्यवाद से पहले से अंतर्जातीय सम्बन्धों के प्रति मौजूद द्वेष को, साम्राज्यवाद के दौरान पुलिस और कानून के रूप में नए सहयोगी मिल गए थे। साम्राज्यवाद के बाद के समय में भी ये सभी द्वेष और बैरभाव साम्राज्यवाद से पहले और फिर साम्राज्यवाद के दौरान की मान्यताओं से ही प्रभावित हैं।
फिर इसके अतिरिक्त, विविधता में एकता की बात करने वाली वह एक विचारधारा हमें यह भी सोचने नहीं देती कि कैसे कुछ विशेष जातियों और वर्गों को चुनकर उन्मुक्त कर देने से दूसरे वर्गों और जतियों की यौनिकता प्रभावित होती है। हाल ही में, एक मित्र ने मुझे फर्स्टपोस्ट (Firstpost) के लिए क्रिस्टीना थॉमस धनराज (Christina Thomas Dhanaraj) द्वारा लिखा हुआ एक लेख भेजा। लेख की लेखिका एक दलित ऐक्टिविस्ट हैं और उनका मानना है कि भारत में नारीवाद में अक्सर जाति सम्बन्धों की वास्तविकता को नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है। यहाँ मैं एक बार फिर से यह दोहराना चाहती हूँ कि ऊंची जाति और ऊंचे वर्ग की महिलाएँ केवल नीची जाति और वर्ग की महिलाओं के त्याग के बल पर ही सशक्त और स्वतंत्र हो पाती हैं। नीची जाति और वर्ग की ये महिलाएँ लगातार मेहनत करते हुए, ऊंची जाति के नारीवादियों के घरों की साफ़-सफ़ाई और उनके बच्चों का लालन पालन करने में लगी रहती हैं। यह बिलकुल साम्राज्यवाद के समय के श्वेत लोगों के उन घरों की तरह ही है जहाँ श्वेत महिलाएँ धीरे-धीरे राजनैतिक मामलों की ओर अग्रसर हो रही थीं और वे ऐसा केवल इसलिए कर पा रही थीं क्योंकि घर पर उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए अश्वेत आया या नौकरानियाँ मौजूद थीं। आज वास्तविकता तो यह है कि, साम्राज्यवाद काल की आया की तरह, ऊंची जाति के लोगों के घरों में काम करने वाली पिछड़ी जाति की महिलाएँ आज भी या तो अपने बच्चों से दूर रहती हैं या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिए जाने के डर से अपने रूमानी सम्बन्धों / सेक्स सम्बन्धों को ताक पर रख देने के लिए विवश होना पड़ता है। जैसा कि धनराज अपने लेख में लिखती हैं, ऊंची जाति की महिलाओं और पिछड़ी जाति की महिलाओं के बीच के अंतर को केवल जान लेने और इसे स्वीकार कर लेने से ही हम एक दूसरे के समर्थन में लगातार खड़ी नहीं रह सकती हैं। इस तरह की जानकारी और स्वीकार्यता से कभी-कभी जाति सम्बन्धों के होने को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है ताकि जेंडर और यौनिक विविधता को दर्शाया जा सके। दरअसल, अंतर-वर्गीयता को जिस रूप में हम समझते हैं, केवल उतना ही काफ़ी नहीं है। हमें ज़रूरत है एक सापेक्ष दृष्टिकोण को अपनाने की जो हमें न केवल यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दे कि नस्ल और जेंडर में केवल अंतर-संबंध मात्र ही नहीं हैं बल्कि ये दोनों एक दूसरे की उत्पाती के कारक भी हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नस्ल और जाति की श्रेष्ठता के बारे में हमारी चिंता ही जेंडर और यौनिकता के बारे में हमारी सोच को प्रभावित करती है। इसी तरह “सामान्य” या “प्राकृतिक” यौन व्यवहारों के बारे में हमारी चिंता ही जाति और नस्ल के बारे में हमारे पूर्वाग्रहों को और मजबूती देती है। भारत में, जहाँ आज जाति और नस्ल की पवित्रता के नाम पर विषमलैंगिकता को ही मान्यता दिए जाने के प्रयास हो रहे हैं, वहाँ एक सापेक्ष नज़रिया अपनाया जाना बहुत श्रेयकर हो सकता है। विषमलैंगिकता पर बल दिए जाने के विरोध करने के लिए केवल हमारा LGBTQI लोगों के अधिकारों के पक्ष में खड़े होना या विविधता का समर्थन करना मात्र ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि हम यह भी जान और समझ लें कि यौनिकता पर नियंत्रण रखने की कोशिशों का सीधा संबंध जाति और नस्ल पर नियंत्रण रख पाने के प्रयासों के साथ होता है।
भारत में हालांकि साम्राज्यवाद के खिलाफ़ लोगों के मन में रोष व्याप्त है, लेकिन फिर भी हमने विविधता को साम्राज्यवाद के पृथक करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए हैं। इसके विपरीत, देश में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ, विविधता भी एक बिकाऊ वस्तु बन गयी प्रतीत होती है। भारत के पर्यटन विभाग ‘अतुल्य भारत’ को एक ऐसे स्थान के रूप में दुनिया के आगे प्रस्तुत करता है जहाँ आने वाला कोई यात्री विविध तरह के लोगों, जानवरों और स्थानों को देख सकता है और भ्रमण कर सकता है। हमारे इन विज्ञापनों में, हमारे टूर गाइड की बातों में, विभिन्न स्थानों के बारे में पर्यटन विभाग के ब्रोशर्स में आज भी साम्राज्यवादी काल की लिखावट आज भी साफ़ नज़र आती है। इन्हीं सब विचारों के चलते भारतीय पुरुष और महिला अक्सर बाज़ार में बिकाऊ वस्तु बने नज़र आते हैं। यहाँ ऊंची जाति के समुदायों में यह ज़्यादा नज़र नहीं आता जहाँ शायद ‘भारतीय परिधानों’ और ‘भोजन’ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन माजुली द्वीप जैसी जगह पर, जहाँ मैं मानवविज्ञान पर शोध करती हूँ, या फिर पूर्वोत्तर भारत में जहाँ अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं, आज भी पर्यटक जनजातिय पुरुष या महिला की शारीरिक बनावट के ‘अंतर’ को देखने के लिए आकृष्ट होते हैं। दरअसल अनेक ऐसी जगहों पर, जहाँ पर्यटन ही लोगों की आय का एकमात्र साधन है, वहाँ के लोग अपने पारंपरिक परिधान पहन कर पर्यटकों का इंतज़ार करते हैं ताकि वहाँ आने वाले पर्यटकों को उनकी जनजाति के लोगों के पौरुष और स्त्रीत्व की ‘वास्तविक’ तस्वीरें मिल सकें।
मुझे लगता है कि विविधता शब्द का प्रयोग छलावे से भरा है। जहाँ सुनने में तो इसमें अनेकता का बोध होता है और लगता है मानों एक से अधिक संभावनाएँ इसमें निहित हैं हालांकि वास्तव में इसका प्रयोग मात्र दो जेंडर भूमिकाओं और विषमलैंगिकता को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। इस शब्द से भिन्नता बहुत अधिक उभर कर सामने आती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए और विविधता के सही अर्थ को फिर से अपनाने के लिए केवल यौनिकता और जेंडर के बारे में शिक्षा देना ही काफ़ी नहीं है बल्कि ज़रूरी है कि दुनिया को नस्लों और जातियों में विभाजित करने में इच्छाओं की भूमिका पर जानकारी दी जाए। इच्छाओं पर एक अलग नज़रिया हमें यह समझने में सहायक हो सकता है कि विविधता या भिन्न होने का अर्थ केवल दुनिया को वर्गों या श्रेणियों में विभाजित करना नहीं है और न ही इसका अर्थ किसी एक नस्ल को दबा कर दूसरी नस्ल की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है। विविधता का सही अर्थ यह जान लेना है अलग-अलग वर्गों और लोगों के बीच के अंतर बिलकुल अस्थायी हैं और ज्यों-ज्यों हम भिन्नताओं को भुला और मान्यताओं को झुठला एक दूसरे के समीप होंगे, यह अंतर खुद-ब-खुद ही धराशायी होते जाएँगे। विविधता के बारे में ऐसे विचार विकसित करने के लिए हमें यह जान लेना होगा कि नस्ल, जेंडर और जाति, सभी एक दूसरे की उत्पत्ति के कारक हैं और इनमें से किसी भी एक को उपनिवेशिता या साम्राज्यवादिता से दूर करने के लिए हमें इनमें से हर एक को मुक्त करना होगा।
सोमेन्द्र कुमार द्वारा अनुवादित
To read this article in English, please click here.